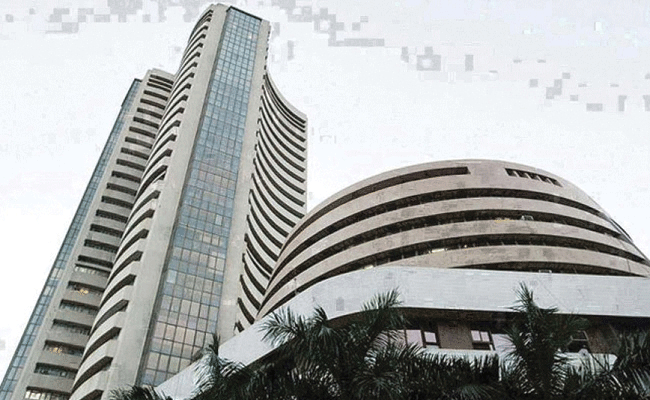भारत में हो रही फास्फोरस की कमी
भारत में हो रही फास्फोरस की कमी
नई दिल्ली। भूमि की उर्वरता की समस्या उतनी ही पुरानी है, जितनी कि कृषि। जब प्रारंभिक मानव ने पहली बार स्थायी कृषि में संलग्न होना शुरू किया, तो उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि फसलों को उनके विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, खेती और कटाई के बार-बार चक्र ने इन पोषक तत्वों को समाप्त कर दिया, जिससे समय के साथ उपज कम हो गई। प्रारंभिक कृषि समाजों ने यह देखना शुरू कर दिया कि कुछ क्षेत्रों में बेहतर फसलें पैदा होती हैं और मिट्टी की भरपाई की जा सकती है।
इस अवलोकन से पौधों और फसल के विकास के लिए आवश्यक मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों को बहाल करने की प्रथाएं शुरू हुईं। दुनिया भर में स्वदेशी समुदायों ने निषेचन के तरीके विकसित किए हैं, उदाहरण के लिए, मछली के अवशेषों और पक्षियों की बूंदों (गुआनो) को उर्वरक के रूप में उपयोग करना।
19वीं सदी में इसमें बदलाव आया, जिससे रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिससे सिंथेटिक उर्वरकों के निर्माण के साथ-साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की पहचान हुई। वे आधुनिक सिंथेटिक रासायनिक उर्वरकों की नींव हैं और इससे कृषि उत्पादकता में उछाल आया है। 20वीं सदी के मध्य की हरित क्रांति ने उच्च उपज वाली फसल किस्मों को अपनाने और इन उर्वरकों के गहन उपयोग को गति दी, और आज ये पदार्थ वैश्विक खाद्य उत्पादन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अब हमारे सामने एक समस्या है। फॉस्फोरस दुर्लभ है और केवल कुछ भूवैज्ञानिक संरचनाओं में सीमित मात्रा में मौजूद है। न केवल हम इससे दूर भाग रहे हैं, बल्कि यह पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। यह गैस के रूप में मौजूद नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह केवल जमीन से पानी में जा सकती है, जहां यह शैवाल के खिलने और यूट्रोफिकेशन की ओर ले जाती है।
फॉस्फोरस का इतिहास गुआनो में इसकी खोज से लेकर वर्तमान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं तक फैला हुआ है। आज मुट्ठी भर देश दुनिया के अधिकांश फॉस्फोरस भंडार को नियंत्रित करते हैं। यह एक प्रमुख भूराजनीतिक चिंता का विषय है। दुनिया का सबसे बड़ा भंडार मोरक्को और पश्चिमी सहारा क्षेत्र में हैं। लेकिन यहां फास्फोरस कैडमियम के साथ सह-अस्तित्व में है, एक भारी धातु जो निगलने पर जानवरों और मानव गुर्दे में जमा हो सकती है। कैडमियम निकालना भी एक महंगी प्रक्रिया है।
परिणामस्वरूप कैडमियम युक्त उर्वरकों को अक्सर मिट्टी में लगाया जाता है, फसलों द्वारा अवशोषित किया जाता है और उपभोग किया जाता है, जिससे हमारे शरीर में जैव संचय होता है। अध्ययनों से पता चला है कि इससे हृदय रोग में तेजी आती है। 2018 में, EU ने उर्वरकों में कैडमियम के स्तर को विनियमित करने के लिए नया कानून पारित किया।
केवल छह देशों में पर्याप्त कैडमियम मुक्त फॉस्फोरस भंडार हैं। उनमें से, चीन ने 2020 में निर्यात प्रतिबंधित कर दिया और कई यूरोपीय संघ के देश अब रूस से खरीदारी नहीं करते हैं, इसलिए सुरक्षित फ़ॉस्फ़ोरस का बाज़ार अचानक विस्फोटित हो गया है। यही एक कारण है कि श्रीलंका ने सिंथेटिक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और 2021 में जैविक उर्वरक अपना लिया, बाद में फसल की पैदावार में अचानक गिरावट का सामना करना पड़ा जिससे राजनीतिक संकट पैदा हो गया।
आज, भारत दुनिया में फॉस्फोरस का सबसे बड़ा आयातक है, इसका अधिकांश हिस्सा पश्चिम अफ्रीका के कैडमियम से भरे भंडार से आता है। सभी फसलें समान दर से कैडमियम अवशोषित नहीं करती हैं, लेकिन धान, भारत की एक प्रमुख फसल, विशेष रूप से अतिसंवेदनशील है। भारतीय किसान धान में बहुत अधिक मात्रा में उर्वरक भी डालते हैं। अन्य अनाज, जैसे गेहूं, जौ और मक्का भी कैडमियम को कम ही अवशोषित करते हैं। इस प्रकार, हमें भविष्य में एक कठिन विकल्प का सामना करना पड़ सकता है: यदि हम फॉस्फोरस से कैडमियम नहीं हटाते हैं, तो हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम ऐसा करते हैं, तो उर्वरक और अधिक महंगे हो जाएंगे।
सबसे पहले खनन किए गए फॉस्फोरस का केवल पांचवां हिस्सा ही वास्तव में भोजन के माध्यम से खाया जाता है। उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण इसका अधिकांश भाग कृषि अपवाह के रूप में सीधे जल निकायों में नष्ट हो जाता है। दूसरा, अधिकांश फास्फोरस जो लोग उपभोग करते हैं वह सीवेज में चला जाता है। भारत में अधिकांश सीवेज का अभी भी उपचार नहीं किया जाता है या केवल माध्यमिक स्तर तक ही उपचारित किया जाता है। इसलिए भले ही कार्बनिक पदार्थ पच जाए, एसटीपी से निकलने वाले अपशिष्ट में अभी भी नाइट्रेट और फॉस्फेट होते हैं। इनमें से, नाइट्रेट्स को डिनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया द्वारा पचाया जा सकता है और नाइट्रोजन गैस के रूप में वायुमंडल में सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सकता है, जबकि फॉस्फोरस तलछट और पानी के स्तंभ में फंसा रहता है। इसके बाद इसे शैवालीय पुष्पों द्वारा अवशोषित किया जाता है जो उच्च पोषक तत्वों की आपूर्ति के जवाब में बढ़ते हैं, और जब वे विघटित होते हैं, तो उन पर फ़ीड करने वाले बैक्टीरिया घुलनशील ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। परिणाम: जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। शैवालीय फूल भी विषैले होते हैं, जिससे उनके संपर्क में आने वाले लोगों को श्वसन संबंधी समस्याएं, मतली और अन्य बीमारियाँ होती हैं।